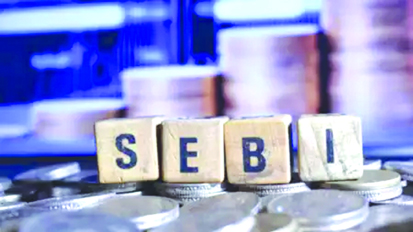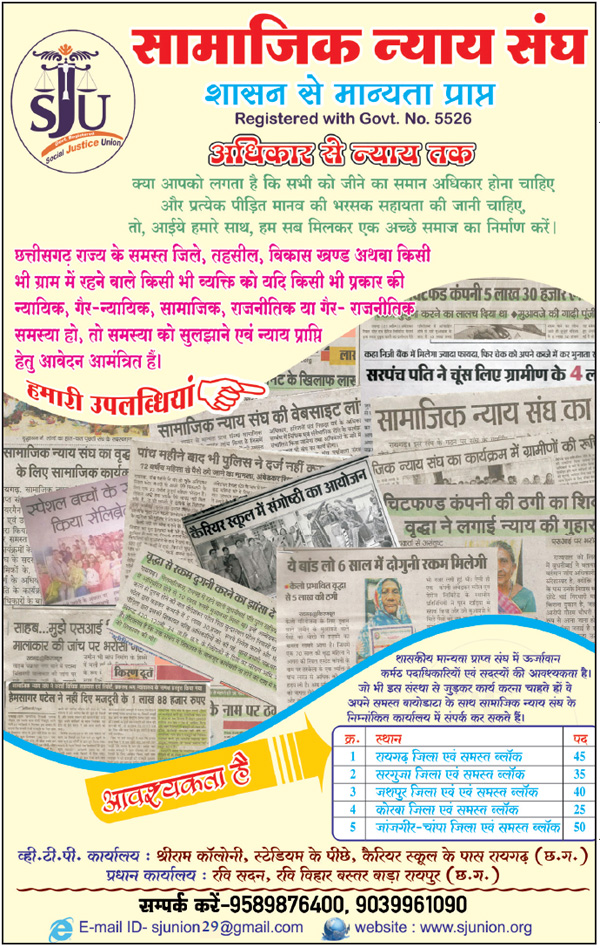व्यापार
एआई का इस्तेमाल करेगा सेबी, 2 साल में 1,000 आईपीओ होंगे प्रोसेस
मुंबई । भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अब कंपनियों द्वारा दायर किए जाने वाले इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करेगा।
सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने मंगलवार को कहा कि आईपीओ के आवेदनों की समीक्षा के लिए नियामक एआई को अपना रहा है। इससे अगले दो साल में 1,000 के करीब आईपीओ प्रोसेस होने की संभावना है। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया (एआईबीआई) के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए बुच ने कहा कि सेबी कंपनियों और उनके मर्चेंट बैंकरों के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड आईपीओ टेम्पलेट पर काम कर रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नया टेम्प्लेट रिक्त स्थान भरें फॉर्मेट में होगा। कोई भी जानकारी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिट नहीं होगी, उसकी बारीकी से समीक्षा के लिए अलग से चिह्नित किया जाएगा।
इस सिस्टम का उद्देश्य आईपीओ दस्तावेजों को दो भागों में विभाजित करना है, जिसमें स्टैंडर्ड और विशेष जानकारी शामिल होगी। सेबी को उम्मीद है कि इससे उसके अधिकारियों के लिए अनियमितताओं की पहचान करना और उनका समाधान करना आसान हो जाएगा। इस पहल से कंपनियों और विनियामकों दोनों के लिए समय की बचत होने की उम्मीद है। एआई तीन प्रमुख तरीकों से मदद करेगा, जिसमें दस्तावेज समीक्षा, ऑनलाइन सर्च और सामग्री जांच शामिल है। बुच के मुताबिक, इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि आईपीओ दस्तावेजों और उनकी समीक्षा करने की दक्षता भी बढ़ेगी। सेबी की विशेष जानकारी रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यकुशलता में और सुधार लाएगी। स्टैंडर्ड और नॉन-स्टैंडर्ड सेक्शन का पालन करके अधिकारी अपनी जांच में प्राथमिकता तय कर सकते हैं जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इससे समीक्षा प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाएगी।
बुच ने कहा, अगले दो वर्षों में 1,000 आईपीओ तक को संभालने की संभावना के साथ यह कदम इसमें शामिल सभी लोगों के कार्यभार को काफी कम कर देगा।
भारत में डेटा सेंटर्स पर खर्च इस साल 19 प्रतिशत बढ़ेगा
नई दिल्ली । भारत में डेटा सेंटर्स पर खर्च 2025 में 19.1 प्रतिशत बढऩे का अनुमान है। यह 2024 की विकास दर से करीब दोगुना है। यह जानकारी मंगलवार को एक पूर्वानुमान में दी गई। गार्टनर के ताजा पूर्वानुमान में बताया गया कि सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज भारत में आईटी खर्च वृद्धि के प्रमुख चालक हैं, जो 2025 में क्रमश: 16.9 प्रतिशत और 11.2 प्रतिशत बढ़ेंगे।
गार्टनर के उपाध्यक्ष विश्लेषक नवीन मिश्रा ने कहा कि सॉफ्टवेयर पर खर्च जेनएआई-सक्षम समाधानों के प्रीमियम कीमत से प्रेरित है। वहीं, आईटी सेवाओं पर खर्च क्लाउडिफिकेशन, डिजिटलीकरण और कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए उद्योगों की आवश्यकताओं के कारण बढ़ रहा है। पिछले महीने रियल एस्टेट कंसल्टेंट सीबीआरई साउथ एशिया की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, भारत के डेटा सेंटर बाजार ने 2019-2024 के बीच घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशकों से 60 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है और 2027 के अंत तक कुल निवेश 100 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है।
गार्टनर के अनुसार, डेटा सेंटर सिस्टम, डिवाइस और सॉफ्टवेयर सहित क्षेत्रों में 2025 में दोहरे अंकों की वृद्धि देखी जाएगी, जिसका मुख्य कारण जनरेटिव एआई (जेनएआई) हार्डवेयर अपग्रेड होना है। पूरी दुनिया में आईटी खर्च 2025 में बढक़र 5.61 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। यह 2024 की तुलना में 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 50 प्रतिशत से ज्यादा सॉफ्टवेयर खर्च जेनएआई से प्रभावित होगा। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की डेटा सेंटर इंडस्ट्री की क्षमता वित्त वर्ष 2026-27 तक दोगुनी बढक़र 2 से 2.3 गीगावाट हो सकती है। इसकी वजह अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन बढऩे के कारण क्लाउड में निवेश बढऩा है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बढ़ती डेटा सेंटर मांग को पूरा करने के लिए अगले तीन वित्त वर्षों में 55,000-65,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है, जो मुख्य रूप से भूमि और भवन, बिजली उपकरण और कूलिंग सॉल्यूशंस पर खर्च किए जाएंगे।
बजट 2025 : रेलवे पर रहेगा खास फोकस, जनता को मिल सकते हैं कई तोहफे
नई दिल्ली । देश का आम बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस बार बजट में रेलवे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और आम जनता के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार के बजट में रेलवे को 2.93 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपये तक का आवंटन किया जा सकता है। यह पिछले साल के मुकाबले 15-20 प्रतिशत अधिक होगा। इस राशि का उपयोग रेलवे के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने में किया जाएगा। स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके तहत यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। देश भर में नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा समय कम होगा।
आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत भी बजट की प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। सरकार का लक्ष्य 2027 तक 68,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विस्तार करना और 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाना है, और बजट में मिलने वाले फंड का उपयोग इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में किया जाएगा।
देश में वर्तमान में रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें सबसे प्रमुख है देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, जिस पर तेजी से काम हो रहा है और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाने की संभावना है। ट्रेनों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए ‘कवच’ नामक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को लगाने का कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए बजट से अतिरिक्त राशि आवंटित की जा सकती है। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई शहरों में मेट्रो रेलवे लाइनों के विस्तार का कार्य भी जारी है और इस विस्तार को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, सरकार वंदे भारत ट्रेनों को बढ़ावा दे रही है और इस साल के बजट में 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों और 100 अमृत भारत ट्रेनों को शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। इन सभी ट्रेनों के संचालन और रख-रखाव के लिए भी बजट से आवश्यक धनराशि आवंटित की जाएगी। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और अधिक सुलभ बनाना है। इस प्रकार, बजट 2025 में रेलवे पर विशेष ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और रेलवे का बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा।
2030 तक कृषि निर्यात का 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य किया जा सकता है हासिल : विशेषज्ञ
नई दिल्ली । विशेषज्ञों ने कहा कि 2030 तक कृषि निर्यात में 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसके लिए स्पष्ट और साहसिक कदम उठाना होगा। यह बात विशेषज्ञों ने कही है।
विशेषज्ञों ने हाल ही में इंफ्राविजन फाउंडेशन की पहल, सेंटर फॉर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड एक्शन (सीएआईआरए) द्वारा दिल्ली में आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करके भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने पर एक गोलमेज सम्मेलन में ये बातें कही।
कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के नेताओं ने गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। इनमें खाद्य प्रसंस्करण सचिव सुब्रत गुप्ता, विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष सारंगी, एसएटीएस इंडिया के कंट्री चेयरमैन सिराज चौधरी, एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव और पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन शामिल थे।
वक्ताओं ने सुझाव दिया कि मौजूदा कृषि अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है, ताकि बड़े पैमाने पर लचीली कृषि पद्धतियों को अपनाया जा सके और भारत के निर्यात को वैश्विक बाजार की बदलती आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके।
खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित उत्पादक-केंद्रित दृष्टिकोण से मांग पर केंद्रित ग्राहक-उन्मुख नीति में परिवर्तन, कृषि निर्यात के लिए अनिवार्य है।
विशेषज्ञों ने कहा कि इसके लिए एक स्थिर और सुसंगत नीतिगत माहौल और एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो निर्यात के लिए लक्षित वस्तुओं और उत्पादन की मात्रा को प्राप्तकर्ता देशों और बाजारों की प्राथमिकताओं और मांगों से मेल खाता हो।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 18.2 प्रतिशत है और 42 प्रतिशत से अधिक आबादी को आजीविका प्रदान करती है, जिससे यह देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन जाती है।
कृषि वस्तुओं का दुनिया का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक होने के बावजूद, भारतीय किसान अवसंरचना और बाजार पहुंच में अंतराल और कमी के कारण कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जबकि भारत निर्यात की कुछ श्रेणियों में बाजार में अग्रणी है।
विशेषज्ञों ने कृषि और समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आह्वान किया। इसके लिए मंत्रालयों में एकीकृत दृष्टिकोण, स्थिर निर्यात नीति वातावरण, कोल्ड चेन, भंडारण और रसद बुनियादी ढांचे का उन्नयन और भूमि के बड़े समूहों में खेती के बीच संतुलन की आवश्यकता है।
इस कार्यक्रम में सीएआईआरए के पहले पृष्ठभूमि पत्र की प्रस्तुति भी हुई। इसमें भारत में उत्पन्न वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे में बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस पत्र में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, कोल्ड चेन नेटवर्क को बढ़ाने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता में सुधार करने के लिए ब्लॉकचेन और आईओटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें दी गईं।
गोलमेज प्रतिभागियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की मौलिक भूमिका पर जोर दिया, लेकिन इसके अतिरेक के खिलाफ भी चेतावनी दी। निजी चुनौतियों के लिए सार्वजनिक समाधानों में सरकारी हस्तक्षेप का संयम से और सटीक रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। कृषि निर्यात को बदलने के लिए आवश्यक मानसिकता परिवर्तनों की ओर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए; महत्वपूर्ण रूप से, नीति क्लस्टरिंग को अपनाना जो विभिन्न सरकारी और उद्योग हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
सीएआईआरए इंफ्राविजन फाउंडेशन (टीआईएफ) की एक पहल है, जिसे अनुसंधान, नीति वकालत और वास्तविक दुनिया के समाधानों के माध्यम से भारत के कृषि-निर्यात परिदृश्य को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
रबी के सीजन में 640 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई फसलों की बुआई
नई दिल्ली । कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, रबी के सीजन में अब तक 640 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में बुआई की गई है। पिछले वर्ष लगभग 637.5 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई की गई थी।
पिछले वर्ष इसी अवधि में 315.63 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस बार गेहूं की कुल बुआई 320 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। इससे इस सीजन में अनाज का उत्पादन बढऩे की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों की बारिश से भी फसल को लाभ मिलने की उम्मीद है।
दलहन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल पिछले वर्ष की इसी अवधि के 139.29 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 141.69 लाख हेक्टेयर हो गया है। इससे दालों की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
श्री अन्ना और मोटे अनाज के तहत 54.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई है, जबकि तिलहन की बुआई 97.62 हेक्टेयर में की गई है।
वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, आने वाले दिनों में खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है और अर्थव्यवस्था के गति पकडऩे की संभावना है। क्योंकि कृषि क्षेत्र को अनुकूल मानसून की स्थिति, बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट की पर्याप्त आपूर्ति से लाभ होने की संभावना है।
सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर पिछले साल दिसंबर में 5.22 प्रतिशत के 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई, क्योंकि महीने के दौरान सब्जियों, दालों और चीनी की कीमतों में कमी आई, जिससे घरेलू बजट को राहत मिली।
अक्टूबर में 6.21 प्रतिशत के 14 महीने के उच्चतम स्तर को छूने के बाद मुद्रास्फीति में कमी लगातार गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाती है। नवंबर में सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 5.48 प्रतिशत रह गई थी। दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट का श्रेय प्रमुख खाद्य वस्तुओं में मूल्य वृद्धि में कमी को दिया गया।
भारत का वार्षिक कॉफी निर्यात बीते 4 वर्षों में दोगुना होकर 1.3 अरब डॉलर हुआ
नई दिल्ली । भारत का कॉफी निर्यात बीते चार वर्षों में करीब दोगुना होकर वित्त वर्ष 2023-24 में 1.29 अरब डॉलर हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 719.42 मिलियन डॉलर था। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को दी गई।
मंत्रालय द्वारा बताया गया कि इसके साथ ही भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है।
जनवरी 2025 के पहले पखवाड़े में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस सहित अन्य देशों को 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया। अपने अनोखे और बेहतर स्वाद के कारण देश के कॉफी निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है।
भारत के कॉफी उत्पादन में लगभग तीन-चौथाई की हिस्सेदारी अरेबिका और रोबस्टा बीन्स की है। इन्हें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि, भुनी हुई और इंस्टेंट कॉफी जैसे वैल्यू एडेड उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे निर्यात में तेजी आ रही है।
मंत्रालय ने बताया कि कैफे कल्चरल के बढऩे, अधिक खर्च योग्य आय और चाय की तुलना में कॉफी के प्रति बढ़ती प्राथमिकता के कारण भारत में कॉफी की खपत भी लगातार बढ़ रही है और यह ट्रेंड शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बढ़ रहा है।
घरेलू खपत 2012 में 84,000 टन से बढक़र 2023 में 91,000 टन हो गई है और यह वृद्धि कॉफी के बढ़ते चलन को दिखाती है।
भारत की कॉफी मुख्य रूप से पारिस्थितिक रूप से समृद्ध पश्चिमी और पूर्वी घाटों में उगाई जाती है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। कर्नाटक उत्पादन में सबसे आगे है, जिसने 2022-23 में 248,020 मीट्रिक टन कॉफी का उत्पादन किया। उसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है।
कॉफी का उत्पादन भारत में सदियों पहले शुरू हुआ था, जब प्रसिद्ध संत बाबा बुदन 1600 के दशक में कर्नाटक की पहाडिय़ों पर सात मोचा बीज लेकर आए थे। बाबा बुदन गिरि ने अपने आश्रम के प्रांगण में इन बीजों को लगाने के उनके सरल कार्य ने अनजाने में ही भारत को दुनिया के प्रमुख कॉफी उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित कर दिया।
अब भारत में कॉफी की खेती एक साधारण प्रथा से विकसित होकर एक संपन्न उद्योग में बदल गई है और भारत की कॉफी को अब दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है।